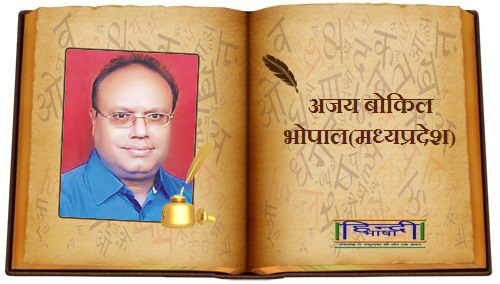अजय बोकिल
भोपाल(मध्यप्रदेश)
******************************************
जाने-माने उद्योगपति राहुल बजाज के निधन पर उनके व्यक्तित्व की कई खूबियों और सत्ता से उनकी करीबी के अनेक प्रसंग दोहराए जा रहे हैं। अस्सी और नब्बे के दशक में देश के सामाजिक बदलाव और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पहचान कर उसे उपभोक्तावाद में भुनाने का काम बजाज ने बखूबी किया है। आर्थिक आकांक्षाएं और जरूरतें सभ्यता के साथ-साथ सांस्कृतिक बदलाव भी लाती है। कभी यह अच्छा भी हो सकता है और कभी खराब भी। इसे थोड़ा और विस्तार दें तो देश में आर्थिक उदारीकरण की औपचारिक शुरूआत और एक उपभोक्ता संस्था के वजूद में आने की नींव १९८० के दशक में जिन २ स्वचालित वाहनों ने रखी थी वो थे-बजाज स्कूटर और मारूित ८०० कार। एक में दावा बुलंद भारत को छूने का था,तो दूसरे में आँखों का सपना साकार होने का था। ये वो दौर था जब छोटे पर्दे के रूप में टेलीविजन मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय घरों में पहुंच रहा था। नई पीढ़ी आधुनिक संचार साधनों को जीवन का जरूरी हिस्सा मानने लगी थी। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन सीमित आय में खटने वाले वाले परिवारों के मन को मथने लगे थे। ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ के उपदेश खोखले लगने लगे थे। भौतिक सुख ही जीवन का सच्चा सुख है, lयह मानने वाली पीढ़ी आकार लेने लगी थी। परंपरागत रूप से एक गरीब,आत्मसंतोषी और आध्यात्मिक भारत पैसे की रंगीन दुनिया में उतराने के सपने देखने लगा।
किसी भी सफल उद्योगपति की पहचान यह है कि वो वक्त की आहट को कितना पहले जान लेता है। सत्तर का दशक आते-आते देश की आजादी के बाद जन्मी पीढ़ी जवान होने लगी थी और स्वतंत्रता संग्राम में अपने बुजुर्गों के त्याग तपस्या की कहानियां सुनकर ऊबने लगी थी। गांधी की सरल और सादगी भरी जीवन शैली का आग्रह मंदा पड़ने लगा था। पूंजीवादी सपनों को साकार करने वाला अमेरिका इस पीढ़ी का नया आदर्श था। हरित क्रांति ने गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी थी। ‘मदर इंडिया’ वाले गांव धीरे-धीरे आधुनिकता की हवा महसूस करने लगे थे। मध्यम वर्ग में सरकारी शालाओं की जगह कान्वेंट संस्कृति का बोलबाला होने लगा था।१९७७ में ‘कोका कोला’ की देश से रवानगी का उल्टा असर यह हुआ कि बाजार ने नए सिरे से हमारे जीवन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इसी के साथ समाजवादी आग्रहों को भी तिलांजलि मिलने लगी। अस्सी के दशक में धार्मिक आग्रह राजनीति में घुलने लगे और बाजार की संस्कृति को तुच्छता से देखने की प्रवृत्ति घटने लगी। मनमाफिक पैसा कमाना और पैसा खर्च करना नैतिक जुर्म नहीं रहा।
समाज के इसी मानसिक और नैतिक बदलाव को २ वाहनों ने रफ्तार दी। हालांकि, इस देश में दोपहिया पहले भी थे और कारें भी थीं,लेकिन मध्यम वर्ग इनसे दूर ही था। पचास के दशक में खुद की एक अदद साइकिल खरीदने के सपने का ‘दि एंड’ अस्सी के दशक में साफ दिखने लगा था। राहुल और उनकी कंपनी ‘बजाज ऑटो लिमिटेड’ ने आंकाक्षाओं के इस बदलाव को अनूदित करने की सफल कोशिश की,जब १९८६ में बजाज का ‘चेतक’ स्कूटर बाजार में आया। रंग-रूप और माफिक रखरखाव से मध्य वर्ग में चेतक खरीदना सामाजिक प्रतिष्ठा बन गया। नौकरी लगते ही युवा चेतक खरीदना अपना कर्तव्य समझने लगे। हालांकि,उस जमाने में लड़कियां आम तौर पर स्कूटर-बाइक नहीं चलाती थीं,लेकिन पति-परिजन या प्रेमी के साथ स्कूटर के पीछे वाली सीट पर बैठकर उड़ते पल्लू या दुपट्टे के साथ हवा से बातें करना नई आजादी का परिचायक बन गया।
दूसरी तरफ चार पहियों वाली मारूति ८०० गाड़ी ‘चेतक’ के ३ साल पहले ही सड़कों पर दौड़ने लगी थी। मारूति ने भी उस उच्च मध्यमवर्ग के अरमानों को पकड़ा,जो पुरानी बुलेट,राजदूत जैसी मोटर साइकिल और वेस्पा,लैम्ब्रेटा जैसे स्कूटरों की दुनिया से आगे निकलना चाहता था। आज की पीढ़ी को शायद भरोसा न हो कि मारूति ८०० की पहली गाड़ी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जारी की थी। पहली गाड़ी सरदार हरपालसिहं ने ४७ हजार ५०० रू. में खरीदी थी,इतने में तो अब स्कूटर भी शायद ही आती हो। जिनके पास दुपहिया गाड़ी थी, वो एक अदद मारूति खरीदकर ‘अमीरों’ की कतार में लगने की जुगत में लगे थे।
तब देश में २ धाराएं साथ चल रही थीं। एक वो वर्ग जो साइकिल से स्कूटर पर आने की जुगत में था और दूसरा वो जिसके पास पहले से दोपहिया थे,वो चौपहिया मारूति पर सवार हो अपना सामाजिक दबदबा बढ़ाने में लगा था। जीवन की नई बुलंदी को छूने के लिए मानो इन तेज रफ्तार वाहनों पर सवार होना जरूरी हो गया था।
बजाज स्कूटर और मारूति की गाड़ी मैकेनिकों और उपभोक्ताओं की दुनिया में मुहावरे बन गए थे। ये २ ऐसी गाड़ी थीं,जो कहीं भी सुधर सकती थीं, जिन्हें कोई भी मैकेनिक ठीक सकता था। सीमित आय में बड़े सपने देखने वाले मध्यम वर्ग को और क्या चाहिए था ?
बजाज स्कूटर और मारूति को लोकप्रिय बनाने में उनके दिल को छूने वाले विज्ञापनों का बड़ा हाथ रहा है। दरअसल,एक उत्पाद बेचने के लिए बनाए गए विज्ञापन कैसे ‘देश का सपना‘ में तब्दील कर दिए जाते हैं,ये मामला उसका बढ़िया उदाहरण है। गोया कि जिंदगी का सच्चा सुख यही है। बजाज के विज्ञापन ने इसी उपभोक्तावादी सपने को बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर में तब्दील कर दिया। बजाज का लक्ष्य समूह मुख्य रूप से निम्न मध्य वर्ग था,जो साइकिल पर चलते थक चुका था। ऐसा स्कूटर जो कीमत में माफिक, दिखने में सुंदर और एकल परिवार के सुखी जीवन के अरमानों को फर्राटे से ले चलने का दावा करता था। यह विज्ञापन टीवी पर १९८९ में दिखने लगा,जब देश में आर्थिकी बदहाल थी और उससे उबरने के लिए आर्थिक उदारीकरण की गरज के तर्क दस्तक देने लगे थे। विज्ञापन में खास तौर से उस निम्न मध्यमवर्ग को लक्षित किया गया था,जो गरीब बस्तियों में रहता था। इस विज्ञापन की पहली लाइन ‘हमारा बजाज’ मानो बदलते मध्यम वर्ग की मुख्य पंक्ति बन गई थी। इस उद्घोष ने मध्यवर्ग की उस हिचक पर विराम लगा दिया कि पैसा कमाना और ऐशो-आराम के लिए उसे खर्च करना बुरी चीज है। इन विज्ञापनों ने मानो गांधी युग के सादगी के सबक भी अल्मारियों में बंद कर दिए। राहुल बजाज के निधन पर आज ४ दशक बाद उन बदलावों को महसूस करना,आकलन करना और वर्तमान संदर्भों में उनके औचित्य को परखना सचमुच दिलचस्प है। जो बदला,उससे देश का कितना भला हुआ,यह बहस का विषय है। आज की तो समूची पीढ़ी उपभोक्तावादी हो चुकी है। ‘किसी भी तरह कमाओ और मनमर्जी से उड़ाओ’ इस पीढ़ी का आदर्श है। अब जबकि सुई से लेकर कार तक शो-रूम में हर वक्त बिकने के लिए उपलब्ध है,ऐसे दौर में कार या स्कूटर का नंबर लगाने के बाद महीनों अथवा बरसों में मिलने वाली उसकी सुपुर्दगी का स्वर्गिक आंनद ये पीढ़ी कभी महसूस नहीं कर पाएगी। बजाज ने एक सुस्त मगर धीरता भरी जिंदगी को अधीर और असंतोषी जीवन तक ले जाने में भी अहम भूमिका निभाई है,इसमें दो राय नहीं।