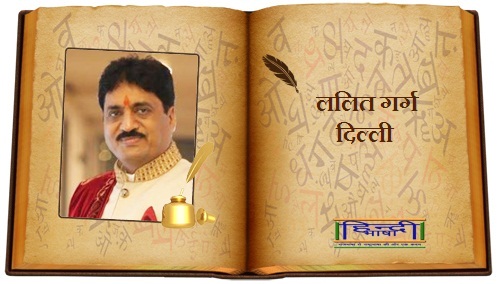दिल्ली
***********************************
जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा यदि भय, हिंसा और दमन का पर्याय बन जाए तो वह सभ्यता की सबसे बड़ी विडम्बना कही जाएगी। हाल के वर्षों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर बढ़ते दबाव, घर और शाला में हिंसक व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ ने शिक्षा की आत्मा पर गहरा आघात किया है। फरीदाबाद की उस हृदयविदारक घटना ने, जिसमें महज गिनती न सीख पाने के कारण एक मासूम बच्ची को पिता की क्रूरता ने मौत के मुँह में धकेल दिया, पूरे समाज को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इस तरह खौफनाक होती पढ़ाई अब केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि जन-जन से जुड़ी विडम्बना बनती जा रही है। इस तथाकथित शिक्षा की विकृत मानसिकता का भयानक परिणाम है कि आज भी यह माना जाता है कि डर-मार से बच्चों को बेहतर बनाया जा सकता है। ज्ञान की इस सदी में यह सोचना ही शर्मनाक है कि पढ़ाई के नाम पर किसी बच्चे से उसका जीवन, बचपन, आत्मविश्वास छीना जा सकता है।
आज शिक्षा धीरे-धीरे मानवीय संवेदनाओं से कटती जा रही है। परीक्षा परिणाम, श्रेणी, अंक तालिका और प्रतिस्पर्धा के आँकड़े शिक्षा का चेहरा बनते जा रहे हैं। अभिभावक अपने अधूरे सपनों का बोझ बच्चों के नाजुक कंधों पर लाद देते हैं और शाला उन्हें प्रदर्शन की मशीन मानकर आँकने लगते हैं। परिणाम यह है, कि बच्चा पढ़ाई को उत्सव या खोज की प्रक्रिया नहीं, बल्कि खौफनाक दायित्व के रूप में देखने लगता है। घर, जो सबसे सुरक्षित और स्नेहपूर्ण स्थान होना चाहिए, वही डर का अड्डा बन जाता है। विद्यालय, जो जिज्ञासा और रचनात्मकता को पंख देने का माध्यम होना चाहिए, वह दंड और अपमान का स्थल बन जाता है। ऐसे में मासूम मन कहाँ जाए, किससे अपने भय और असहायता को साझा करे। मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के तमाम अध्ययन यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हिंसा, डांट, डर और अपमान बच्चों की सीखने की क्षमता को नष्ट करते हैं। डर के माहौल में बच्चा न तो प्रश्न पूछ पाता है, न प्रयोग कर पाता है, न ही अपनी गलतियों से सीख पाता है। उसकी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और निर्णय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धीरे-धीरे वह हीनभावना का शिकार हो जाता है और स्वयं को अयोग्य समझने लगता है। यह कुंठा केवल बचपन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे जीवन उसके व्यक्तित्व पर छाया की तरह मंडराती रहती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर भी जोखिम लेने से डरते हैं, अपनी बात रखने में संकोच करते हैं और जीवन की प्रतिस्पर्धा में आत्मविश्वास के अभाव में पिछड़ जाते हैं। यह शिक्षा नहीं, बल्कि एक तरह का मानसिक शोषण है।
हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर बच्चे को एक ही मापदंड से आँकना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर बच्चा अपने-आपमें विशिष्ट है। किसी की रुचि गणित में है तो किसी की कला में, कोई खेल में खिलता है तो कोई संगीत या साहित्य में। प्रकृति ने हर बच्चे को किसी न किसी विशेष क्षमता के साथ भेजा है, लेकिन हम उसे पहचानने की बजाय एक तयशुदा पाठ्यक्रम और अपेक्षाओं की बेड़ियों में जकड़ देते हैं। नई शिक्षा नीति-२०२० ने बहुआयामी शिक्षा, रुचि आधारित सीख व मूल्यपरक दृष्टि की बात जरूर की है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी अंक और श्रेणी की मानसिकता हावी है। कोचिंग संस्कृति, बोर्ड परीक्षाओं का भय और प्रवेश परीक्षाओं की दौड़ ने शिक्षा को और भी संकीर्ण बना दिया है, साथ ही यह भी एक कटु सत्य है कि कई बच्चे जन्मजात, आनुवंशिक या परिस्थितिजन्य कारणों से सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। दृष्टि दोष, श्रवण समस्या, डिस्लेक्सिया, मानसिक तनाव या पारिवारिक अस्थिरता जैसी स्थितियाँ उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे बच्चों को सबसे अधिक समझ, धैर्य और सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वही बच्चे सबसे पहले डांट और दंड का शिकार बनते हैं। शिक्षक और अभिभावक उनकी समस्या को समझने की बजाय उन्हें आलसी या अयोग्य ठहरा देते हैं। यह रवैया न केवल अमानवीय है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के साथ अन्याय भी है।
शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना है। यदि शिक्षा अहिंसा, करुणा, सहानुभूति और आत्मसम्मान का पाठ नहीं पढ़ाती, तो वह अधूरी है। बच्चों को सिखाने का सबसे प्रभावी माध्यम उदाहरण होता है। जब वे घर और शाला में संवाद, धैर्य और प्रेम देखते हैं, तभी वे वही मूल्य आत्मसात करते हैं। भय के वातावरण में पले बच्चे या तो दब्बू बन जाते हैं या फिर हिंसा को ही समाधान मानने लगते हैं। समाज में बढ़ती असहिष्णुता और आक्रामकता के पीछे कहीं न कहीं वही शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है, जो संवेदनशील मनुष्यों के बजाय केवल प्रतिस्पर्धी उपभोक्ता तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बार-बार परीक्षा के तनाव को कम करने और शिक्षा को जीवन से जोड़ने की अपील इस बात का संकेत है कि समस्या गंभीर है, लेकिन केवल भाषणों और नीतियों से बदलाव नहीं आएगा। असली परिवर्तन तब होगा, जब अभिभावक यह समझेंगे कि उनका बच्चा उनकी प्रतिष्ठा का साधन नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। जब शिक्षक यह मानेंगे कि उनका दायित्व केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि बच्चों में सीखने की ललक जगाना है। जब विद्यालय प्रशासन दंड की संस्कृति छोड़कर सहयोग और परामर्श की व्यवस्था विकसित करेगा, और जब समाज यह स्वीकार करेगा कि असफलता भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई अपराध नहीं।
आज जरूरत है शिक्षा को फिर से मानवीय बनाने की। ऐसी शिक्षा की, जिसमें ‘स्नेह’ अनुशासन का आधार हो, ‘संवाद’ दंड का विकल्प बने और ‘विश्वास’ भय की जगह ले। बच्चों को यह एहसास कराया जाए कि वे जैसे हैं, वैसे ही स्वीकार्य हैं और उनकी प्रगति का रास्ता उनकी अपनी गति से तय होगा। शिक्षा को अहिंसक दृष्टि से देखना केवल नैतिक आग्रह नहीं, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता भी है। क्योंकि जिस समाज की शिक्षा बच्चों को तोड़ती है, वह समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। मासूमों को डर नहीं, हौसले का संबल चाहिए; डांट नहीं, दिशा चाहिए; और हिंसा नहीं, विश्वास चाहिए। तभी शिक्षा सचमुच जीवन देने वाली बन सकेगी, जीवन लेने वाली नहीं।
आज चिंताजनक प्रश्न यह है कि जो शिक्षा जीवन निर्माण, चरित्र गठन और मानवीय मूल्यों के संवर्धन का माध्यम होनी चाहिए थी, वही धीरे-धीरे विध्वंस का कारक क्यों बनती जा रही है ? जब शिक्षा सही दिशा में आगे नहीं बढ़ती, जब वह अहिंसा, करुणा, सह-अस्तित्व और नैतिक विवेक से सम्पन्न नागरिकों का निर्माण करने में विफल रहती है, तब उससे निकलने वाली पीढ़ियाँ केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी संकट का कारण बनती हैं।