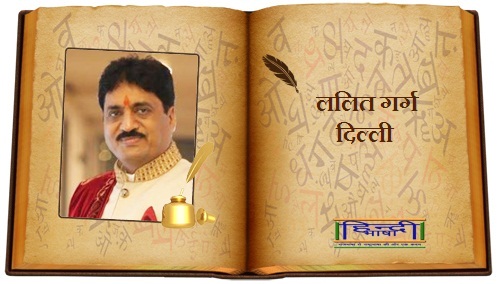दिल्ली
***********************************
बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों ही गठबंधनों ने बढ़-चढ़कर लोक-लुभावनी और जनता को आकर्षित या गुमराह करने वाली घोषणाओं से जुड़े चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं। जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, वे निश्चित रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। यह प्रश्न अब गंभीर हो गया है कि क्या घोषणा पत्र लोकतंत्र के महाकुंभ यानी चुनाव का सबसे सशक्त हथियार बन चुके हैं या चुनावी छलावा ? निश्चित ही यह जनता को रिझाने और प्रभावित करने का प्रमुख माध्यम बन गया है, परंतु सत्ता में आने के बाद कितने राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों का अक्षरशः पालन किया है, यह बड़ा सवाल है। वास्तव में घोषणा पत्र किसी दल का दृष्टिपत्र होता है, जो उसके विचारों, उद्देश्यों और संकल्पों का सार्वजनिक दस्तावेज है। यह बताता है कि दल सत्ता में आने के बाद राज्य या देश की दिशा कैसी तय करना चाहता है, किन मूलभूत समस्याओं का समाधान करना चाहता है और विकास की कौन-सी राह पर चलना चाहता है। घोषणा पत्रों में किए गए वादों को लेकर परस्पर विरोधी दलों में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तो छिड़ता है, लेकिन उन्हें लेकर वैसी सार्थक बहस नहीं हो पाती, जैसी विकसित देशों में होती है और जिसके आधार पर स्वस्थ जनमत तैयार करने में मदद मिलती है। हैरानी नहीं, कि अपने यहाँ चुनावी घोषणा पत्र अपनी महत्ता खोते जा रहे हैं।
लोकतंत्र में घोषणा पत्र की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह मतदाताओं के लिए जानकारी और निर्णय का आधार बनता है। मतदाता यह जान सकते हैं, कि कौन-सा दल किस विषय पर क्या सोचता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और वह किन वर्गों के कल्याण के लिए क्या योजनाएं रखता है। यह राजनीतिक दलों की जनता के प्रति सार्वजनिक प्रतिज्ञा होती है, एक तरह की जवाबदेही का प्रतीक, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय लोकतंत्र में यह जवाबदेही सिर्फ कागजों पर ही रह गई है। अधिकांश दल चुनाव जीतने के बाद घोषणा पत्रों को भूल जाते हैं। मतदाता भी अपने मत के बदले वादों की पूर्ति का हिसाब नहीं मांगते। परिणामस्वरूप घोषणा पत्र एक औपचारिकता और दिखावे का माध्यम बनकर रह गए हैं। इतिहास पर नजर डालें तो अधिकांश घोषणाओं का पालन आधा-अधूरा ही हुआ है। राजस्थान में पिछली सरकार ने अपने घोषणा पत्र के लगभग ६४ प्रतिशत वादे पूरे किए, जबकि कर्नाटक में सिर्फ ३ प्रतिशत वादे ही पूरे हुए। यह बताते हैं कि घोषणा पत्र को गंभीरता से न तो दल लेते हैं, न जनता। यह स्थिति लोकतंत्र की आत्मा के विपरीत है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल करे और जवाब मांगे।
घोषणा पत्रों की एक बड़ी समस्या यह है कि उनमें की गई घोषणाएं वित्तीय दृष्टि से असंभव होती हैं। जनता को खुश करने के लिए ऐसे वादे किए जाते हैं, जिनके लिए न तो संसाधन हैं, न ठोस योजना। कोई कानूनी प्रावधान भी नहीं है कि दल अपने वादे पूरे न करने पर जवाबदेह बने। यही कारण है कि चुनाव के बाद घोषणाएं भुला दी जाती हैं। बिहार चुनाव के संदर्भ में देखें तो एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अत्यधिक आकर्षक और लोक-लुभावन वादों से भरे घोषणा पत्र जारी किए हैं। एनडीए ने अपने ‘संकल्प पत्र’ में १ करोड़ नौकरियों का वादा किया है, महिलाओं को २ लाख रुपए तक की सहायता, हर जिले में कौशल केंद्र, किसानों के लिए ९ हजार ₹ वार्षिक सम्मान निधि और ७ नए एक्सप्रेस-मार्गों के निर्माण की बात कही है, तो महागठबंधन ने अपने ‘तेजस्वी प्रण’ में प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी देने, महिलाओं को ढाई हजार ₹ मासिक सहायता, २५ लाख ₹ का स्वास्थ्य बीमा, २०० यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी और मंडियों की बहाली जैसे बड़े वादे किए हैं। दोनों घोषणाओं में एक बात समान है- वे अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी और जन-लोभक हैं। नौकरियों, मुफ्त बिजली, नकद सहायता और भारी निवेश की घोषणाएं सुनने में तो आकर्षक लगती हैं, पर इनकी व्यावहारिकता संदिग्ध है। बिहार जैसे राज्य में, जहां संसाधन सीमित हैं और रोजगार की स्थिति जटिल है, इन वादों को लागू करना आसान नहीं है। घोषणाओं में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इतने बड़े खर्चों का वहन कैसे होगा, कौन-से विभाग या योजनाएं इनका संचालन करेंगे और कब तक परिणाम दिखेंगे।
इन घोषणा पत्रों में जनकल्याण की भावना अवश्य है, परंतु वह यथार्थ से अधिक कल्पना पर आधारित लगती है। बिहार की वास्तविक समस्याएं- शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवासी मजदूर, कृषि संकट, रोजगार और उद्योगों का अभाव, इनका समाधान केवल लोक-लुभावन वादों से नहीं होगा। आवश्यक है कि दल घोषणाएं करने से पहले उनकी वित्तीय और प्रशासनिक व्यवहार्यता का गंभीर अध्ययन करें। राजनीति में घोषणा पत्रों का उपयोग अब एक चुनावी हथियार के रूप में हो रहा है, न कि जनसेवा की प्रतिबद्धता के रूप में। मतदाता को भी जागरूक होना होगा कि वे केवल वादों से प्रभावित न हों, बल्कि यह जानने की कोशिश करें कि पिछले चुनावों में किए गए वादों में से कौन-से पूरे हुए। मीडिया और सामाजिक संस्थाओं को भी यह दायित्व निभाना चाहिए, कि वे चुनावों के बाद घोषणाओं की निगरानी करें, ताकि दल जवाबदेह बनें। घोषणा पत्र तभी सार्थक होंगे, जब उनमें किए गए वादे मापनीय, समयबद्ध और संसाधन-सिद्ध हों। दलों को चाहिए कि वे घोषणाओं को नारेबाजी के बजाय ठोस योजनाओं में बदलें। यह भी आवश्यक है, कि चुनाव आयोग इस दिशा में कोई नीति बनाए ताकि असंभव और अव्यावहारिक वादों से जनता को भ्रमित न किया जा सके।
जब कोई पार्टी चुनाव जीत कर सत्ता में आती है तो सवाल उठता है कि क्या वह घोषणा-पत्र जो एक अनुबंध का रूप ले चुका है, उसे लागू होना चाहिए या नहीं ? जिस सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के तहत सरकारें चुनी जाती हैं, क्या किए गए वादों को पूरा करने के संदर्भ में उनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए ? चुनाव आयोग को भी इस बारे में नए सिरे से विचार करना चाहिए, ताकि इसका कुछ ठोस समाधान किया जा सके। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, कि घोषणा पत्र लोकतंत्र के महाकुंभ में जनता को प्रभावित करने का सबसे सशक्त माध्यम हैं, परंतु जब तक वे केवल वादों की झड़ी बने रहेंगे और उनके पालन की कोई बाध्यता नहीं होगी, तब तक यह लोकतंत्र की सार्थकता को अधूरा रखेंगे। बिहार के दोनों गठबंधनों के घोषणा पत्र लोकतांत्रिक उत्सव की चमक तो बढ़ाते हैं, पर उनका सच समय के साथ ही सामने आएगा कि वे जनता की उम्मीदों को पूरा करते हैं या सिर्फ चुनावी छलावे साबित होते हैं।