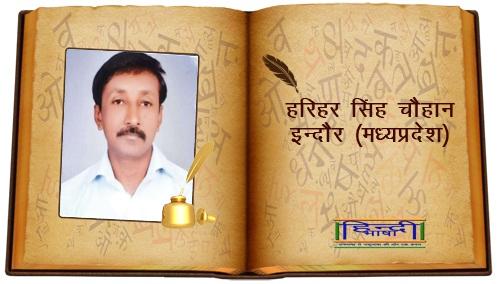हरिहर सिंह चौहान
इन्दौर (मध्यप्रदेश )
************************************
सुख में या खुशियों की इस अमर बेला में हर कोई अपने अपने घरों की ओर बढ़ता जा रहा है। हम और हमारी आस्था में जो संस्कृति व सभ्यता के अनुरूप एक तरह के अपनेपन वाली बात होती है। वह पर्व, खुशियों, त्योहारों की मस्ती और परिवार के साथ हम सभी का लगाव, मानो सम्पूर्ण परिवार हमारा अपना है। यही इस बात को उजागर करता है कि एकजुटता में सम्मान मिलता है। तभी तो जैसे ही हम हमारे शहर पहुंचे, तो मानो बहुत दिनों बाद अच्छा वातावरण और जुड़ाव महसूस हुआ। तभी पास वाले भैय्या दयाराम जी कहते हैं, “अरे बबलू, कब आए तुम महानगर से भैय्या!”
“बस भैय्या अभी अभी आ ही रहा हूँ।”
“अच्छा कैसा चल रहा है ?”
“भैय्या सब ठीक है, पर महानगरों की भाग-दौड़ में वह चिंतन नहीं है। सभी दौड़ रहे हैं हर पल।”
“हाँ बबलू, यह बात तो ठीक है। तुम बहुत सही बात कह रहे हो। हम भी अखबारों में इस पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति में इन महानगरों की संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ बहुत सूनापन होता है, बड़े-छोटे फ्लैट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अड़ोस-पड़ोस के लोग एक-दूसरे को पहचानते ही नहीं हैं भाई। उन चारदीवारी में घरों का स्नेह व वात्सल्य नहीं है, वहाँ सिर्फ मकान है घर नहीं। अपना किसे कहें महानगरों की संस्कृति में! लोगों को सिर्फ अपनी चिंता है, दूसरों से कोई लेना-देना नहीं। यहीं मनुष्य का मतलबपरस्त स्वरूप सामने आता है। जहां ना पेड़ों की छाँव है और ना मानवता, ना कोई किसी के सुख-दु:ख का साथी, सिर्फ दिखावा ही दिखावा है। वहाँ तो बेगानों की तरह दिनचर्या की सुबह-शाम और रात बीत जाती हैं, जहाँ आदमी अकेला ही है।”
“हाँ भैय्या, इसी लिए तो परम्परागत भारतीय संस्कृति, सभ्यता के त्यौहारों व पर्वों पर हम सभी को अपने गाँव व छोटे शहरों की याद आ ही जाती है। अपने गली-मोहल्लों की यादें ही हमें खींच लाती है। जीवन के वह पल जो बचपन से युवावस्था की दहलीज पर हम लोगों ने बिताए थे, वह चिंतन के साथ मंथन की सार्थक संवाद की एकजुटता है। फुर्सत में जब सब काम निपट जाता है, तो घरों के बाहर आज भी रिश्तेदारों व दोस्तों की गोष्ठी शुरू होती है, और उन्हीं ओटलों पर हमारे बड़े-बुजुर्ग के अनुभव की ढाल हमारी हर परेशानी एवं सुख-दु:ख में मददगार साबित होती है। आपस में समन्वय, मैत्रीपूर्ण भाव, सकारात्मक चर्चा, प्रेम, निष्ठा और समर्पण के सूत्रों में जब परिवार एक-साथ मिल कर ओटलों पर चर्चा करते थे, तो मानो खुशियाँ तथा सुख-समृद्धि सभी आसपास ही रहतीं थीं, पर जैसे- जैसे भोगवादी पश्चिमी संस्कृति का रंग और आधुनिकता आई, उस कलेवर ने हमें अपनों से दूर कर दिया। वह हँसी, मज़ाक-ठहाकों का सागर चारदीवारी में सिमट गया, मकान, फ़्लैट व बिल्डिंगों में बंध गया। आज-कल लोग मोबाइल, कम्प्यूटर, लेपटॉप और टेलीविजन तक उस सुकून को तलाशते दिखाई देते हैं। सही बात है दया भैय्या, आजकल शरीर की चिंता महानगरों में ज्यादा होती है, क्योंकि आराम व सुख के चक्कर में यहाँ परिश्रम और मेहनत को आराम व आलस से हम लोगों ने तोड़ दिया और मशीनों के गुलाम बन गए। पैदल चलना छोड़ दिया। तभी तो मुस्कान को ढूंढने शहरों के लोग सुबह-सुबह बाग बगीचों में ठहाके लगाते हैं, गाते- मुस्कराते हैं, पर वह एक तरह की दिनचर्या कृत्रिम साँसों के समान ही है। जब तक हमारे हृदय में संवेदनाएं व मानवीय मूल्यों का जागरण नहीं होता, तब तक सब बेकार ही है। वर्तमान समय में फिर पुराने दिनों का पर्दापण कब होगा, क्या फिर वह दिन लौट के आएंगे ?, जब ओटलों पर फिर हम सभी बैठेंगे। वह दिन, वह खुशी के पल ना जाने कहाँ गए, गली-मोहल्लों में अब कहाँ खो गए वह ओटले ? वर्तमान में तलाश तो ज़ारी रहना चाहिए सुकून की, क्योंकि भोगवादी विचारों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, जबकि पारम्परिक एकजुटता के साथ मिल-जुलकर बातचीत से ही हर समस्या का हल निकलता है। वह चिंतन से ही सम्भव है, जब फुर्सत के पलों में हम अपने घरों के बाहर बाहर ओटलों पर बैठकर संवाद करेंगे, क्योंकि चिंतन से ही समाधान का रास्ता निकलता है और पुराने दिनों की बातों का वजन आज भी है।