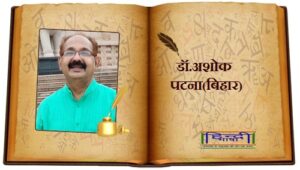शशि दीपक कपूर
मुंबई (महाराष्ट्र)
*************************************
मनुष्य को आस-पास का परिवेश सदैव प्रभावित करता है। किसने किस समुदाय से क्या सीखा, यह अपने स्वभाव पर निर्भर करता है और फिर वह सबके स्वभाव के अनुकूल कैसे हो जाता है ? क्या भाषा इस अनुकूलता में सहायक बनती है या धर्म-जाति के उठे असामयिक विवाद ? भाषा में मातृभाषा की संवेदनशीलता अन्य भाषाओं के बनिस्बत अधिक रहती है। आज समाज में दो ही विधियों से भाषा विचार व भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन है-मातृभाषा और अंग्रेज़ी। हिंदीं को व्यावहारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन शालेय शिक्षा व कार्यालयी या व्यवसायिक शिक्षा में अंग्रेजी सर्वोपरि है। माता-पिता द्वारा बच्चों को जितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए दे रहे हैं। बच्चे इस स्वतंत्रता से क्या सीख रहे या सिखा रहे हैं, नि:संदेह, यह सामाजिक क्रिया का भविष्यात्मक प्रतिक्रिया परिणाम ही होगा।
“मनुष्य श्रद्धा अथवा साहस किसी दूसरे से उधार नहीं ले सकता है।” समाज आज श्रद्धा व साहस की पराकाष्ठा के उस पार पहुँच चुका है। प्रत्येक स्वयं को निर्दोष व दूसरे को दोषयुक्त बताने में जुटा है। महात्मा गांधी जी ने मातृभाषा और अंग्रेज़ी भाषा के प्रति अपनी निजी श्रद्धा व साहस से संवेदनाएँ व भावनाएं गुजराती के गुजराती में और अंग्रेज़ी जाननेवालों के साथ अंग्रेज़ी में बनाए रखी, ऐसा उस समय के महान व्यक्तित्व वाले लोगों व राजनेताओं का सहज साधन भी साबित हुआ। मातृभाषाएं छई-मुई पौधे की तरह पनपती हैं। सहजता, कोमलता, सरलता व सहृदयता उसमें अनुवांशिक रची-बसी होती है।
“भाषा प्रयोग व अनुकरण की वस्तु है।” अत: मातृभाषा सीखते हुए संसारभर की किसी भी भाषा को सीखने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते भाषा का प्रयोग समाज और राष्ट्र हित के लिए हो रहा हो।
मनुष्य किसी स्थिति विशेष में किस हद तक जा सकता है ? यह तथ्य उतना गंभीर कदापि नहीं बन सकता, जब तक उसमें ‘शुद्ध चित्त मंत्र’ जुड़ा हो। भाषा व मातृभाषा सामान्य सामाजिक व्यवस्थाओं के नियमों को ओढ़ कर फलती हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ़्रीका में तमाम निवासियों के चित शुद्ध के लिए भजन हिंदी, गुजराती व अंग्रेज़ी में गाए। भाषा व मातृभाषा संबंधी विवाद केवल व्यक्तिवादी अंहकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजभाषा पुस्तकों में छापने या गठित स्मृतियों, यदा-कदा मंत्रालयों व सरकारी विभागों में एक भाग बनाने या वार्षिक उत्सव का संसाधन बनाने में सही दिशा अक्सर नहीं हो सकती। हाँ, श्वाँस लेती अवश्य दिखाई पड़ सकती हैं, लेकिन उन्नति की दृष्टि से अभी भी कोसों दूर है। राष्ट्र भाषा हिंदी को संवैधानिक दर्जा देने में विलम्ब होने का स्थाई कारण भी दृष्टव्य नहीं होता है। जो विरोध करते हैं, उनकी ही मातृभाषा में संस्कृत भाषा ७०-८० प्रतिशत शब्द हैं। संस्कृत हिंदी में तत्सम रूप में शब्द गृहीत करती है, तो फिर हिंदी के प्रति आए-दिन होते विवादों का कारण क्या हो सकता है ? मात्र अपनी प्रभुसत्ता के औचित्य को प्रस्तुत करने के सिवाय!
प्रत्येक भाषा का अपना स्वरूप है, और उसकी अपनी संवेदना व भावना प्रस्तुति के लिए शब्दों के ताने-बाने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज़ी का प्रचलन है और राष्ट्रभाषा में हिंदी ही देश की एक पोशाक है। संपूर्ण देश में सर्वधर्म जाति के लोग हिंदी व्यावहारिक तौर समझते व बोलते हैं। अत:, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में विलम्ब करना देशहित में किसी अर्थ में उचित नहीं है। दुनियाभर के कई राष्ट्रों ने अपनी भाषा को संवैधानिक श्रेणी में रखकर देश की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया। उन देशों की भाषाएँ सीखने के लिए लोग लाखों रूपए ख़र्च कर वहाँ जाकर सीखते हैं। देश के लिए विदेशी आय प्राप्त होती है और राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक गर्व अनुभव करता है। काश! कुछ ऐसा ही हमारे देश में हो जाए, भले ही दिल्ली दूर सही, लेकिन कोशिश करनेवालों की हार कभी नहीं होती है।