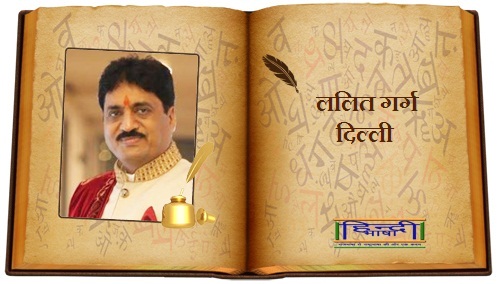दिल्ली
***********************************
भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर समय-समय पर प्रश्न खड़े होते रहे हैं। शिक्षा की विसंगतियों एवं दबावों के चलते भी अनेक सवाल खड़े हैं। इन्हीं से जुड़ा यह एक बेहद हृदय विदारक और चिंताजनक तथ्य है कि एक वर्ष देश में लगभग १४ हजार शालेय बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इस तथ्य की पुष्टि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भी कर रहा है। अधिक घातक तथ्य यह है कि बीते १ दशक में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में लगभग ६५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष २०१९ की तुलना में यह संख्या ३४ प्रतिशत अधिक है। यह केवल आँकड़े नहीं हैं, बल्कि उन मासूम सपनों की समाधियाँ हैं जिन्हें हमारी शिक्षा प्रणाली ने दम तोड़ने पर विवश कर दिया। यह स्थिति किसी एक विद्यालय, राज्य या परिस्थिति की नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा तंत्र की विफलता का दर्पण है। पहली नजर में इतनी बड़ी संख्या में आत्मघात के मूल में पढ़ाई का दबाव, अभिभावकोें की अतिश्योक्तिपूर्ण महत्वाकांक्षाएं, छात्रों की संवेदनशीलता और तंत्र की नाकामी बताई जा सकती है, लेकिन सवाल है कि हमारा तंत्र क्यों संवेदनहीन बना हुआ है ? यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को तलब करके इस बाबत विस्तृत विवरण मांगा है, साथ ही सवाल पूछा है कि क्या देश के सभी शिक्षण संस्थान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी निभा रहे हैं ? शिक्षा को प्रतिस्पर्धा का रणक्षेत्र कब तक बनने दिया जाता रहेगा ?
आज का विद्यार्थी बचपन से ही एक ऐसी अंधी एवं प्रतिस्पर्धी दौड़ में धकेल दिया जाता है, जिसमें लक्ष्य अंक, श्रेणी, और स्तर बन गए हैं-ज्ञान, संवेदना और चरित्र नहीं। विद्यालय अब शिक्षालय नहीं, बल्कि परीक्षा-केंद्र यानी गला-काट प्रतियोगिता के केन्द्र बन चुके हैं। माता-पिता, शिक्षक और समाज-सभी ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है, जहाँ ‘सफलता’ का अर्थ केवल चिकित्सक, अभियंता, आईएएस या उच्च वेतन वाली नौकरी तक सीमित हो गया है। शिक्षा अब व्यक्ति के भीतर के मनुष्यत्व, रचनात्मकता और संवेदना को विकसित करने का माध्यम नहीं रही, बल्कि उसने जीवन को ‘प्रदर्शन की प्रतियोगिता’ बना दिया है। छोटे बच्चों पर कोचिंग का बोझ, अभिभावकों की अपेक्षाएँ, और असफलता का भय ?-ये त्रिकोणीय दबाव उन्हें धीरे-धीरे मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। शिक्षा अब एक बोझ और मानसिक तनाव का कारण बन गयी है।
ब्यूरो के आँकड़े बताते हैं कि छात्रों में आत्महत्या के प्रमुख कारण हैं-परीक्षा में असफलता, अभिभावकीय दबाव, भविष्य की चिंता और मानसिक अवसाद। भारत दुनिया के उन शीर्ष देशों में शामिल है, जहाँ किशोरों में अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। कबीर ने कहा था-“पढ़ि-पढ़ि पंडित भया, पर भीतर का मन ना गया।” आज की शिक्षा बच्चों को केवल ‘जानकार’ बना रही है, ‘ज्ञानी’ नहीं। विद्यालयों में रट्टामार संस्कृति, अंक-केंद्रित मूल्यांकन और शिक्षकों की संवेदनहीनता बच्चों के भीतर आत्मविश्वास के बजाय भय भर रही है। कई प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर्स में तो यह प्रवृत्ति और विकराल हो जाती है। कोटा, पटना, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में हर वर्ष दर्जनों विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। विडंबना यह है कि वहाँ शिक्षा से ज्यादा ‘प्रतियोगिता का उद्योग’ पनप गया है। बच्चे अपने परिवारों से दूर, दबाव और भय में जीते हैं, और अंततः जीवन से हार जाते हैं।
साल २०२० में आई नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत उम्मीदें थीं कि शायद यह शिक्षा को बच्चों के बोझ से मुक्ति देगी, उसे रचनात्मकता और नैतिकता से जोड़ेगी। नीति में ‘होलिस्टिक लर्निंग’, ‘जॉयफुल एजुकेशन’, ‘रिड्यूस्ड बोर्ड प्रेशर’ जैसे शब्द तो हैं, पर व्यवहारिक स्तर पर हालात में कोई ठोस परिवर्तन नहीं आया। परीक्षा का दबाव जस का तस है, महाविद्यालयों में बेरोजगारी का डर और कोचिंग की होड़ बढ़ी है। शिक्षा नीति के भीतर आत्महत्या जैसे मानसिक स्वास्थ्य संकट पर कोई गंभीर विमर्श नहीं हुआ। जब तक शिक्षा नीति का केंद्र मानव-निर्माण नहीं होगा, तब तक यह प्रणाली केवल आँकड़े बढ़ाएगी-आत्महत्याओं के भी और बेरोजगारों के भी। सवाल यह भी है कि शैक्षणिक परिसरों में आत्महत्या रोकने के लिए जो कदम केंद्र व राज्य सरकारों को उठाने चाहिए थे, उसके बाबत देश की शीर्ष अदालत को क्यों पहल करनी चाहिए ? इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए सर्वाेच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि केंद्र व राज्य सरकारें ८ सप्ताह के भीतर वह विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करें, जो आत्महत्या रोकने के दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।
शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी ने कहा था-“शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का सम्यक विकास।” स्वामी विवेकानंद ने भी कहा “शिक्षा वह है जो व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मसंयम और आत्मबल भर दे”, परंतु आज की शिक्षा न शरीर को स्वस्थ रख पा रही है, न मन को शांत, न आत्मा को ऊँचा। बच्चों को किताबों के बोझ तले दबा दिया गया है, पर जीवन की समझ नहीं दी गई। उन्हें बताया गया कि असफलता अपराध है, जबकि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक तो असफलता ही होती है। माता-पिता और शिक्षक दोनों को यह समझना होगा कि बच्चा कोई प्रोजेक्ट नहीं, एक जीवित आत्मा है। उसे सफलता के साँचे में ढालने से पहले उसे अपने ढंग से खिलने का अवसर देना जरूरी है। शिक्षक यदि केवल अंक देने वाले बन जाएँ और अभिभावक केवल रिपोर्ट कार्ड से बच्चे की योग्यता मापें, तो बच्चे का आत्मसम्मान कुचलना निश्चित है। जरूरी है कि घर और विद्यालय दोनों जगह भावनात्मक संवाद स्थापित हो-जहाँ बच्चा अपनी असफलता, डर और उलझन को बिना भय के साझा कर सके।
जब तक बच्चों को यह नहीं सिखाया जाएगा कि जीवन अंक-पत्र से बड़ा है, तब तक यह संकट बना रहेगा। विद्यालयों में ध्यान, योग, संवाद, कला, संगीत और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए। सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, संवेदना-केंद्रित संस्कृति गढ़नी होगी।
देश में मोटी पगार वाली नौकरियों की गला-काट स्पर्धा में शिक्षण संस्थाएं व शिक्षक उस दायित्व को भूल गए हैं, जो छात्रों को विषयगत शिक्षा के साथ विषम परिस्थितियों के बीच जीवन जीने की कला सिखा सके। उन्हें व्यावहारिक जीवन का कौशल सिखाने के साथ ही चुनौतियों से जूझने की मानसिक शक्ति विकसित करने के लिए तैयार कर सकें। आखिर किसी परिवार की उम्मीद को किस स्थिति में यह सोचना पड़ता है कि मौत को गले लगाना अंतिम विकल्प है ? निस्संदेह, शिक्षण संस्थानों का एक मात्र लक्ष्य किताबी ज्ञान देकर उपाधि बांटने तक ही नहीं हो सकता।यह प्रश्न अब टालने योग्य नहीं रहा कि क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उन्हें धीरे-धीरे तोड़ रहे हैं ? शिक्षा यदि आत्महत्या का कारण बन जाए, तो उससे बड़ा विडंबनापूर्ण पराजय कोई नहीं। जरूरत है ऐसी शिक्षा की जो बच्चों को जीवन से प्रेम करना सिखाए, न कि जीवन से भागना। निस्संदेह, देश के शालेय छात्रों में आत्मघात की प्रवृत्ति राष्ट्र की गंभीर क्षति है, जिसे संवेदनशील ढंग से दूर करने की तत्काल जरूरत है।