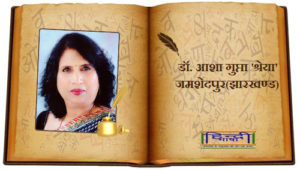अजय बोकिल
भोपाल(मध्यप्रदेश)
*****************************************************************
फिल्म बनाना और उसका चलना न चलना बेशक एक व्यवसाय है,लेकिन कुछ अच्छी और सोद्देश्य फिल्मों का न चलना अथवा कम चलना समाज की संवेदनशीलता और समझ पर भी सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या समाज फिल्मों के आईने में अपनी मनपसंद या चयनित छवि ही देखना चाहता है ? पिछले हफ्ते प्रदर्शित हुई और प्रदर्शन से पहले ही विवादों में फंसी दीपिका पादुकोण और मेघना गुलजार की फिल्म ‘छपाक्’ पहले हफ्ते में बाॅक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। पहले हफ्ते के संग्रहण आँकड़ों से लगता है कि समीक्षकों की अनुकूल टिप्पणियों के बावजूद फिल्म लागत भी जैसे-तैसे निकाल पाए, जबकि उसी के साथ प्रदर्शित हुई अजय देवगन की फिल्म ‘तानाजी:द अनसंग वाॅरियर’ बाॅक्स आॅफिस पर भी खूब तलवारें चमका रही है। पहले सप्ताह में इसने सौ करोड़ का आँकड़ा पार कर लिया है और सिनेमाघरों में यह दर्शकों को अभी भी खींच रही है। विषयवस्तु,कालखंड और सामाजिक सरोकारों के हिसाब से दोनों अलग-अलग तरह की फिल्में हैं। दोनों की आपस में सीधी तुलना करना भी गलत होगा। अलबत्ता ‘छपाक्’ बनाने में एक बड़ा व्यावसायिक जोखिम पहले से निहित था,फिर भी दीपिका और मेघना ने उसे उठाया। तेजाबी हमले (एसिड अटैक) से विरूपित स्त्री की यह संघर्ष गाथा है। इस फिल्म को प्रबुद्ध दर्शकों ने देखा और सराहा भी। फिर भी वह ‘कल्ट’ फिल्म बनकर रह गई। दूसरी तरफ ‘तानाजी’ में मराठा महानायक शिवाजी के वीर सेनापति तानाजी के शौर्य और मूल्य निष्ठा की रोमांचक कहानी है,जो लोगों में देशप्रेम और समर्पण के भाव का संचार करती है। दोनों की लागत में भी तीन गुने का फर्क है।
इन फिल्मों को लेकर राजनीति और सोशल मीडिया में बहिष्कार और पुरस्कार की मुहिमें भी चलीं। इसके राजनीतिक रंग को और गहरा करने के लिए कुछ राज्यों ने अपने-अपने आग्रहों के हिसाब से फिल्म को कर मुक्त(टैक्स फ्री) किया,जबकि दोनों ही फिल्में इस लायक हैं। दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म के प्रचार के लिए दिल्ली में जेएनयू जाकर अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन और एनआरसी का विरोध कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई। परिणामस्वरूप बुद्धिजीवियों का एक वर्ग दीपिका के साथ खड़ा दिखाई दिया,लेकिन इस विचार के समर्थक लोग भी फिल्म देखने थियेटर तक कितने गए,यह भी एक सवाल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों को दीपिका का यह रुख नागवार गुजरा और इसी को राजनीतिक रूप देते हुए ‘छपाक्’ के बहिष्कार की घोषणा कर दी गई। उसे देखने को ‘देशद्रोह’ से जोड़ने की अवांछित कोशिश भी हुई। इसका भी फिल्म के कारोबार पर कुछ न कुछ गलत असर हुआ।
वैसे बाॅलीवुड में अच्छी,सार्थक और ‘समय से आगे’ कही जाने वाली फिल्मों के भी बाॅक्स आॅफिस पर औंधे मुँह गिरने के उदाहरण पहले से मौजूद हैं। ये फिल्म ‘कालजयी’ तो कहलाईं,पर अपने वर्तमान में असफल मानी गईं। उदाहरण के लिए गुरूदत्त की क्लासिक फिल्म ‘कागज के फूल’ हो या राज कपूर की ‘मेरा नाम जोकर’,महान गीतकार शैलेन्द्र की ‘तीसरी कसम’ हो या फिर यश चोपड़ा की ‘सिलसिला‘,ये सब कला की दृष्टि से बेहतरीन और नवोन्मेषी होने के बाद भी कमाई के मामले में ‘गंवाई’ ज्यादा साबित हुईं, क्योंकि आम दर्शकों ने उन्हें हाथों-हाथ नहीं लिया। इस मामले में कमाल अमरोही की अमर फिल्म ‘पाकीजा’ की अलग ही मिसाल है। ‘पाकीजा’ शुरू में बुरी तरह असफल रही, लेकिन उसी दौरान फिल्म की नायिका और महान अभिनेत्री मीना कुमारी की असमय मौत ने उनकी ‘पाकीजगी’ को फिल्म की रिकाॅर्ड तोड़ कामयाबी में बदल दिया। मीना कुमारी तो इस फानी दुनिया से चली गईं,लेकिन दर्शकों ने ‘पाकीजा’ को हमेशा के लिए अपने सीने से लगा लिया। ‘जोकर’ जैसी यादगार फिल्म व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और दर्शकों की बदलती रूचि का शिकार हो गई। लोगों ने ‘मेरा नाम जोकर’ की जगह ‘जानी मेरा नाम’ को बहुत ज्यादा पसंद किया। दिलचस्प बात ये है कि यहां फिल्म के शीर्षक के जरिए दोनों नायक अपनी पहचान जता रहे हैं,लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग-अलग है।
यहां बुनियादी सवाल यह है कि ‘छपाक्’ जैसी फिल्में व्यावसायिक कसौटियों पर खरी क्यों नहीं उतरतीं,और दूसरा यह कि जीवन के रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को लोग फिल्मी पर्दे पर जस का तस देखना अमूमन क्यों पसंद नहीं करते ? ‘छपाक्’ के सिनेमाघरों में अपेक्षानुरूप न चलने का श्रेय लेने का दावा वो मंडली ले रही है,जिसने इसके बहिष्कार की मुहिम चलाई थी,लेकिन आम दर्शक उससे कितना प्रभावित हुआ यह बताना मुश्किल है,फिर भी कुछ असर तो हुआ ही होगा। इसी के साथ यह भी सच है कि बहुत से दर्शक जो ‘छपाक्’ देखने जाने की सोच भी रहे थे,वो भी अाखिरी क्षणों में इरादा बदल बैठे। इसका मूल कारण शायद फिल्म में दिखाई गई वो कड़वी और मन को खिन्न कर देने वाली सच्चाई है,जो सच होते हुए भी रजतपट पर नहीं भाती। यानी ऐसी फिल्म को देखना स्वर्ग के किसी थियेटर में नर्क पर केन्द्रित नाटक देखने जैसा है। और यह भी कि दर्शक किसी सुंदर स्त्री का अस्तित्व के लिए संघर्ष तो पर्दे पर कौतुक भाव से देख सकते हैं,लेकिन किसी कुरूप बना दी गई स्त्री का संघर्ष उनमें में वैसी सहानुभूति नहीं जगाता,जो किसी फिल्म को खासा ‘कमर्शियल ब्रेक’ दे सके,भले ही इस अन्याय और पाशविकता के लिए खुद समाज दोषी हो,समाज की व्यवस्थाएं दोषी हों। यहां तक कि स्वयं महिलाएं भी ऐसी किसी महिला के संघर्ष को पर्दे पर साकार होते देखने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं दिखाई पड़तीं,जो उनके सपनों के काल्पनिक संसार को उध्वस्त करता हो। मनुष्य के इस मनोविज्ञान का राजनीति से कोई खास लेना-देना नहीं है,क्योंकि मनुष्य मूलत: सुंदरता का उपासक है,विद्रूपता का नहीं।
दूसरे शब्दों में-यह भाव कुछ-कुछ वैसा ही है कि सभी लोग इलाज के लिए अस्पताल जाना तो पसंद करते हैं,लेकिन शायद ही कोई स्वेच्छा से उस अस्पताल के ‘बर्न वार्ड’ या ‘मर्चुरी’ में जाना चाहता हो। वहां भी मनुष्य ही होते हैं,लेकिन उनके जीवन से सौंदर्य की आभा छिन चुकी होती है या फिर जिदंगी एक बंद घड़ी में तब्दील हो चुकी होती है।
‘छपाक्’ व्यावसायिक रूप से भले उतनी न चले,लेकिन इस फिल्म को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा,क्योंकि इसके लिए निर्माता और नायिका ने कई स्तरों पर खतरे उठाए, इस बात का अंदाजा होते हुए भी कि जनआंदोलनों के साथ खड़े होना और भीड़ से हटकर जोखिम भरे विषय पर फिल्म बनाना व्यावसायिक सफलता की गारंटी नहीं है,पर खतरे वही लोग उठाते हैं,जिनमें साहस होता है। सिक्कों की खनक से मानव संवेदनाओं की झंकार ज्यादा बड़ी है। इसकी गूंज दूर तक जाती है। पैसा जेब भर सकता है,उत्पीड़न की खलिश को नहीं भर सकता। ‘छपाक्’ का सबक यही है कि दीपिकाओं को निराश नहीं होना चाहिए। अभी समाज में बहुत से त्रासद चेहरे हैं,जिनका दर्द उजागर करना बाकी है।