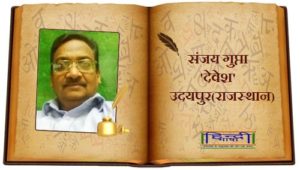शशि दीपक कपूर
मुंबई (महाराष्ट्र)
*************************************
रचना का हस्ताक्षर-भाग २
(स्वप्न में विचरते बेबस कवि व ईमानदार आलोचक के बीच हो रहे संवाद का अगला अंश…)
कविवर थे जो मनमौजी। उन्हें तो कवि बन छा जाने की फ़िक्र ज़्यादा थी,साथ ही मान-सम्मान की तीव्र लालसा धन प्राप्ति के लिए भी। उनका अपना बाल-बच्चों सहित साधारण आकांक्षाओं से घिरा परिवार था। वे उनके लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्थाओं के दृढ़-संकल्पित सात-फेरे लिए जुगाड़ के साथ चल रहे थे।
उच्चतम साँस से प्राणायाम करते हुए मन मसोस कर कविवर ने अभी अर्ध-स्वर ही उच्चारित किया था ,’संस्..कृ…। आलोचक ने तेज़ी से उस शब्द पर ही झपटा बाज़ की भाँति मार लिया और बताने लगे, “संस्कृत का प्राय: सारा पद्य समूह बिना बन्दी का है और संस्कृत से बढ़कर शायद ही और किसी भाषा में हो।“
‘और हाँ! अब तुम मुझसे कहीं यह न पूछना कि भरतमुनि,वामन,दण्डी,अभिनव गुप्त आदि प्राचीन आचार्यों के इस संबंध में क्या मत हैं ? इतना ज्ञान एक कविवर को रचना रचने से पहले होना आवश्यक है। बंधु! बिना साहित्य ज्ञान के रचनाएं तो शब्दों का भंडार हैं और मूल्य कबाड़ी के पास पड़ी रद्दी हैं। यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी अपने साहित्य निबंध में लिख कर प्रमाणित कर चुके हैं। सब समकालीन आलोचक इनके सिद्धांत को सिर आँखों पर अपने चश्मे के नंबर में गढ़,कान पर ऐंठ चढ़ा रचना के तत्वों की ऐसी-तैसी छानबीन करते हैं कि रचना अपने मूल रुप से टुकड़े-टुकड़े होकर पुनः नई संवेदना की साँस में जन्म ले लेती है। यानी कि आज की रचनाएं पाश्चात्य की देन आलोचना के वस्त्र पहन लोकप्रिय हो जाती हैं,जबकि भक्ति काल की रचनाएं आलोचना क्षेत्र से बाहर रहकर लोकसहृदयी बनने में सफल रहीं हैं।
कविवर तो कुछ ओर पूछना चाह रहे थे,मगर राह में ‘संस्कृत’ पता नहीं कहाँ से आ गई ? अब ‘कर्ता ( मरता की जगह)क्या न करता’ के मुहावरे से जूझते हुएव्याकुल हो पुन: अपनी शंका निवारण हेतु बोले, ‘मान्यवर! यह तो बताइए,मेरे मन में प्रतिदिन उड़ान भरने के लिए ‘विचार स्वतंत्रता’ में बड़ी बाधा आती है। थोड़ा रुक कर, ..कृपया कतिपय उपाय हो तो बताइए।”
आलोचक दीर्घ स्वर में कहने लगे, ‘हाँ…हाँ…, …. “विचार-स्वतंत्रता’ में बहुत बाधा आती है जब तुम तुले हुए शब्दों में कविता और तुक अनुप्रास ढूँढने लगते हो।”
ये तो कुछ नहीं महाशय कविवर ! “पद्य के नियम कवि के लिए एक प्रकार की बेड़ियाँ हैं। तुम भी उसकी जकड़ में हो ”,प्यारे !’
आलोचक को कविवर के मायूस मुख देख थोड़ी सहानुभूति हुई,ढाँढस बाँधते-बँधाते फिर कह उठे, “….उनसे जकड़ जाने से कवियों को अपनी स्वाभाविक उड़ान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में,आप अपने मनोभावों को स्वाधीनतापूर्वक प्रकट करें।“
कविवर गहरी साँस लेते हुए ज्यों ही करवट लेने लगे,आलोचक ने आगे हाथ बढ़ा कर रोक दिया। कहने लगे, ‘भाई,तुम मेरी बात को अनसुना क्यों कर रहे ? मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ,और तुम हो…कि !’
कविवर ने मूँदी हुई आँखों पर खिड़की के परदों से छन-छन आ रही स्ट्रीट लाइट को चादर की ओट में छुपाकर कहा, ‘महोदय ! पद्य रचना रचने में क्या कमी रह गई हमसे ? जो अब तक न तुलसीदास बन पायीं,न ही कबीर,न रहीम,न ही रसखान,और तो और भूषण और बिहारी की ‘सतसई’ के इर्द-गिर्द भी न घूम सकी। माथे पर हाथ पटके हुए कहने लगे कविवर, … न छायावादी,न प्रयोगवाद,न प्रगतिवादी, ना ही प्रगतिवाद से जुड़ा शब्द ‘जनवादी।’ बस,मेरी रची रचना, तो…किसी वाद में फ़िट नहीं हो रहीं, सोच रहा हूँ,छद्म नाम अशोक कुमार वर्मा की बजाय अशोक निठल्ला कर लूँ,केवल वर्ग ही बदलेगी,जाति-धर्म तो नहीं न ! वैसे भी एक रचनाकार के लिए यह सब बातें कहाँ महत्व रखती हैं ? उसे तो केवल रचना रचने तक से ही मतलब होता है,उसका ध्येय केवल ज्ञान अर्जन करना-कराना होता है,और वह अपनी रचनाओं में कुछ नयापन ला सके। कविवर ‘न काहु से दोस्ती,न काहु से बैर’ के मन्तव्य को धारण कर ‘सब जाति-धर्म में समन्वय को‘ ही महत्वपूर्ण मानता है।…’
(प्रतीक्षा कीजिए अगले भाग की…)