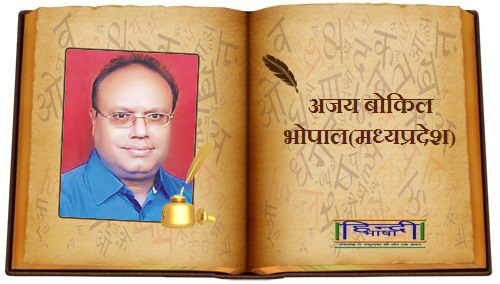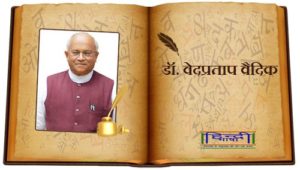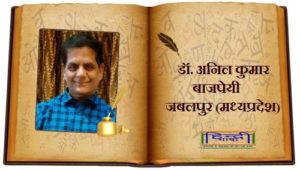अजय बोकिल
भोपाल(मध्यप्रदेश)
******************************************
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुरू नानक जयंती और देव दिवाली पर उनकी सरकार द्वारा देश में लागू ३ विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा,इन कानूनों के खिलाफ सालभर से आंदोलन कर रहे किसानों की नैतिक जीत तो है ही,साथ में यह प्रमं श्री मोदी का दूरगामी राजनीतिक दांव भी है। यह लोकतंत्र में जनता के आगे झुकने की विवशता भी है और एक कदम पीछे हटकर दो कदम आगे बढ़ने की चाल भी है। मोदी का जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बचाए रखने का उपक्रम भी है और विपक्ष से ऐन चुनावी युद्ध के पहले एक अहम मुद्धा छीन लेने का दांव भी है। हाल के उपचुनावों के नतीजों में छिपी चेतावनी को समझने की कोशिश भी है और उप्र के आसन्न विधानसभा चुनाव में विपरीत परिणामों की संभावना को नकारने का सियासी शिष्टाचार (या व्यवहार)भी है। यह फैसला राजनीतिक अंहकार को लगी ठेस भी है और इस ठसक को जज्ब कर नई बिसात बिछाने की चतुराई भी है। कुल मिलाकर इस बहुत बड़े राजनीतिक फैसले के कई कोण हैं। वरना सालभर पहले जो प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील कर रहे थे और कृषि कानूनों को हर हाल में उनके हित में बता रहे थे,वही प्रमं माफी मांगते हुए आज अपनी ही ‘तपस्या’ की सार्थकता पर शंकित हो रहे हैं।
यकीनन,विवादित कानूनों की वापसी सालभर से गर्मी,ठंड और बरसात की चिंता किए बगैर और मोटे तौर पर अहिंसक आंदोलन चलाने वाले किसानों की साधना का सुफल है। इस दौरान आंदोलन को बदनाम करने की हरसंभव कोशिश हुई। इसे कभी आढ़तियों द्वारा पोषित तो कभी खालिस्तान समर्थकों का आंदोलन कहा गया। कहा गया कि यह बड़े किसानों के स्वार्थों का आंदोलन है। इसे दबाने और डेरे-तंबू उखाड़ने की भी पुरजोर कोशिश की गई। आंदोलन को मिल रहे आर्थिक और नैतिक समर्थन पर सवाल खड़े किए गए। इस आंदोलन के कारण परेशान आसपास के लोगों के अधिकारों की बात की गई। यह भी कहा गया कि यह सिर्फ पंजाब,हरियाणा और पश्चिमी उप्र के किसानों का आंदोलन है। इसे जाट असंतोष से भी जोड़ा गया, आंदोलनकारी देशविरोधी तक बताए गए। आंदोलन को खारिज करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने कृषि कानूनों को ‘किसान हितैषी’ बताने वाली रैलियां भी निकालीं। यह भी सच है कि यह किसान आंदोलन देश के बाकी राज्यों में उस तरीके से नहीं फैला, जैसा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे राज्यों में फैला। इसके पीछे रणनीतिक कारण भी हो सकते हैं।
बहरहाल,इन कानूनों की वापसी की घोषणा के साथ यह सवाल फिर मौजूं है कि आखिर सरकार इन कानूनों को लेकर क्यों आई थी ? ऐसी कौन-सी मजबूरी थी कि देश के ११ करोड़ किसानों से बगैर व्यापक विचार-विमर्श के कोरोना काल में ताबड़तोड़ ये संसद में पारित करने पड़े ? इसकी मांग किसने की थी ? अगर ये इतने ही किसान कल्याणकारी थे तो किसानों के गले ये बात क्यों नहीं उतरी ?
ये ३ कानून बीते साल १७ सितंबर को संसद में ताबड़तोड़ पारित किए गए थे। इनमें पहला है-कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य(संवर्धन और सुविधा) विधेयक २०२०। इसके मुताबिक किसान देश भर में बिना किसी रूकावट के मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। दूसरा-मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक २०२०। इसके जरिए देशभर में अनुबंध खेती की व्यवस्था लागू करना है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं,बल्कि अनुबंध करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। तीसरा है-आवश्यक वस्तु संशोधन बिल,जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ में खाद्य तेल,तिलहन,दाल,प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से जमा सीमा हटा दी गई है।
जब इन कृषि कानूनों का देश में विरोध शुरू हुआ, लगभग उसी समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत अमेरिका व्यापार परिषद में अमेरिकी कंपनियों को ‘आत्मनिर्भर भारत’ में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे थे। क्या यह सिर्फ संयोग था ? इसका एक कोण विश्व व्यापार संगठन का ‘कृषि करार’ भी है। इसका उद्देश्य सभी सम्बन्धित देशों में बिना किसी रूकावट यानी कृषि के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके लिए जरूरी है कि सम्बन्धित देश अपने यहां कृषि अनुदान खत्म करें। यही कृषि अनुदान विकसित और विकासशील देशों के बीच कृषि व्यापार में ‘कबाब में हड्डी’ की तरह है। यह अनुदान एमएसपी,कृषि संरक्षणवादी नीतियों और कृषि उत्पादों के आयात निर्यात में करों में छूट के माध्यम से दिया जाता है। भारत सरकार पर विकसित देशों का दबाव है कि वो अपने किसानों से कृषि उत्पाद न खरीदे। हालांकि,भारत सरकार ने इस पर आपत्ति उठाई है,लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव अपने तरीके से काम करते हैं। इसमें दादागिरी यह है कि विकसित देश अपने किसानों को तो भरपूर अनुदान देंगे,लेकिन विकासशील देशों को ऐसा करने से रोकेंगे,ताकि वो विकसित देशों से कृषि माल खरीदने पर विवश हों। कृषि कानून लाने के पीछे यह दबाव भी रहा है।
ऊपरी तौर पर तीनों कृषि कानून किसानों के हित में लगते हैं,लेकिन इनसे जुड़ी आशंकाएं और कुछ व्यावहारिक अनुभव इनके किसान हितैषी होने के दावों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। किसानों को डर है कि नए कानून वास्तव में निजी कंपनियों के हाथ में खेती देने और किसानों को उनके भाग्य पर छोड़ देने के लिए हैं। पुराने जमींदारों की जगह कारपोरेट कंपनियां ले लेंगी। इसी प्रकार अगर माल कृषि उपज मंडियों से बाहर खरीदने-बेचने की व्यवस्था होगी तो शुरू में व्यापारी अच्छे भाव में खरीदेंगे,बाद में बाजार पर उनका नियंत्रण होते ही दाम गिरा देंगे और किसान रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। मप्र में अतीत में सहकारी तिलहन संघ की मौत इसका स्पष्ट उदाहरण है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं मिलेगा तो किसान की लागत भी नहीं निकल पाएगी,मुनाफा तो दूर की बात है। दूसरे,देश में ८६ फीसदी छोटे किसान हैं और ज्यादा शिक्षित भी नहीं हैं। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि,वो दूर-दराज की मंडियों तक माल ले जाकर ऊंचे दाम में बेचें और बेहतर भाव मिलने तक इंतजार कर सकें। हालांकि,इस आशंका को निरस्त करने के लिए सरकार ने सीधे किसानों से माल खरीदने और ऑनलाइन भुगतान का तोड़ निकाला,लेकिन फिर भी जो शंकाएं थीं,वो निरस्त नहीं हुई है। उसी तरह अनुबंध खेती कानून भी कंपनियों के हित में माना गया,जिसमें किसानों के हितों की रक्षा का पक्ष कमजोर था। इन तमाम आशंकाओं का सरकार के पास कोई समाधानकारक जवाब नहीं था। हालांकि,कृषि अर्थशास्त्री मोदी सरकार के फैसले को आर्थिक सुधारों की दृष्टि से प्रतिगामी कदम मान रहे हैं।
जाहिर है कि,अगर कानून पूरी तरह किसानों के हित में थे तो उन्हें ताबड़तोड़ पास करवाने की क्या मजबूरी थी ? जब ये सरकार अपने हर एजेंडे की व्यापक कथा( विवरण)बनाने में माहिर है तो कृषि कानून लाने के पीछे कौन-सा दबाव था ? खासकर तब कि, जब कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान को हम अन्नदाता कहते नहीं अघाते,लेकिन जब कानून बनाने की बात आती है तो उसे ही भरोसे में लेना क्यों जरूरी नहीं माना गया ? इस दृष्टि से सरकार का अपने ही फैसले को वापस लेना उसकी नैतिक हार है। प्रधानमंत्री ने इतना तो माना कि,वो और उनकी पार्टी तमाम कोशिशों के बाद भी किसानों को समझा नहीं पाई कि ये कानून उनके हित में कैसे हैं ? लोकतंत्र में सरकार का जनमत के आगे झुकना कोई शर्म का विषय नहीं है। तंत्र का लोक के आगे नतमस्तक होना ही लोकतंत्र की ताकत है। इसके पहले भी सरकार अपना भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून,पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार अपराधी सांसदों और विधायकों को बचाने वाला विवादास्पद कानून और राजीव गांधी की सरकार प्रेस के खिलाफ मानहानि कानून वापस ले चुकी है।
तो क्या इन कृषि कानूनों की वापसी मोदी सरकार का राजनीतिक विवशताजन्य फैसला है ? किसानों को नाराज करके कोई सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। यकीनन,उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड और पंजाब राज्य के विधानसभा चुनाव इसके पीछे बड़ा कारण हैं। सरकार और भाजपा को इस बात के संकेत मिल गए थे कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा चुनाव में बड़ा गुल खिला सकता है। इसलिए इन्हें वापस लेने में ही भलाई है। अचानक फैसले से हतप्रभ विपक्ष इसे ‘मोदी के अहंकार की हार’ भले बता रहा हो,लेकिन उसके सामने अगला संकट किसी बड़े चुनावी मुद्दे की तलाश होगा,क्योंकि किसानों के एक बड़े वर्ग का गुस्सा खुद-ब-खुद ठंडा हो जाएगा और इसके मोदी विरोध में तब्दील होने की संभावना बहुत घट जाएगी। वैसे भी तमाम नकारात्मक कारणों के बावजूद मोदी भक्ति में कोई बहुत कमी आई है,ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी। विधानसभा चुनाव तक कृषि कानूनों का मुद्दा लगभग खत्म हो चुका होगा।
उधर,भाजपा उप्र में विकास के दावों के साथ अपनी मूल साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति पर निश्चिंतता से लौट सकेगी। दूसरी तरफ,पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस की असमाप्त अंतर्कलह के चलते राज्य में चुनाव के पहले एनडीए के पुराने साथी भाजपा और शिरोमणि अकाली दल फिर साथ आ सकते हैं। अब इसमें कै.अमरिंदरसिंह का कोण भी जुड़ सकता है। उत्तराखंड में शायद ज्यादा फर्क न पड़े। अभी इस खेल का एक अध्याय समाप्त हुआ है,दूसरा बाकी है। ऐसे में अगर भाजपा कृषि कानून वापस लेकर उप्र में अपनी ताकत कायम रखकर अगले लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली पर भगवा फहरा पाती है,तो मोदी की यह माफी भी सस्ती ही पड़ेगी!