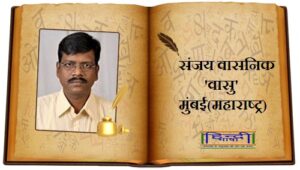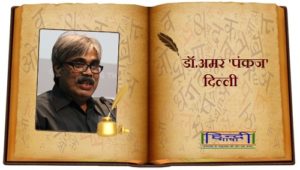डॉ.एम.एल.गुप्ता ‘आदित्य’
मुम्बई (महाराष्ट्र)
**********************************************************
नव-वर्ष और विश्व हिंदी दिवस………
`मन की बात` अपनों से न कहूँ तो किससे कहूँ ? शायद कुछ लोग मेरी बात से सहमत न हों,मुझसे रुष्ट हो जाएँ,भला-बुरा कहें। हो सकता है कि वे ही सही हों,पर मैं तो अपने मन की ही कह सकता हूँ। जो देखता हूँ,जो देख रहा हूँ,वही कह सकता हूँ। जैसे-जैसे देश में हिंदी के नाम पर अनुष्ठानों में वृद्धि होती जा रही है,वैसै-वैसे हिंदी की स्थिति कमजोर होती जा रही है। हालांकि,भारत के अनेक कथित आशावादी हिंदी प्रेमी बड़ी ही बुलंद और ऊंची आवाज में मंचों पर इस बात को यह कह कर नकारने की कोशिश करते हैं,और ऐसा करते हुए उनके चेहरे पर आई चमक और आत्मविश्वास से ऐसा लगता है कि उनके सिंहनाद से हिंदी पूरे ब्रह्मांड की धूरी बनती जा रही है। यह आज की बात नहीं,पच्चीस-तीस साल पहले भी यही आलम था।
मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे तेवर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का सबसे आसान तरीका है कि संकट को स्वीकार ही न करो। जब संकट है ही नहीं,तो उससे निपटने के लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। हिंदी के गीत गाओ,अनुष्ठान करो, माल-पूड़ी खाओ। हिंदी के प्रसार का उनका यह उद्घोष कुछ वैसा ही होता है जैसा कि पाकिस्तान का यह कहना कि करगिल सहित भारत से हुए सभी युद्धों में उसकी जीत हुई। `सर्जिकल स्ट्राइक` या अन्य किसी मुठभेड़ में उनका कभी कोई सैनिक मारा ही नहीं गया,लेकिन सच्चाई तो हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी है। जो हिंदी के अध्यापक-प्राध्यापक गर्मजोशी से यह कहते हैं कि हिंदी तेजी से आगे बढ़ रही है,वे अच्छी तरह जानते हैं कि अब उनके विद्यालय-महाविद्यालय में हिंदी अध्ययन की क्या स्थिति है। अब हिंदी विषय में कितने और कौन विद्यार्थी दाखिला लेते हैं ? कितने विषय उनके यहाँ हिंदी माध्यम से पढ़ाए जाते हैं ?
लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति और अंग्रेजों के तमाम प्रयासों के बाद स्वतंत्रता के समय और उसके कुछ समय बाद तक भी भारत में प्रायः लगभग सभी लोग मातृभाषा में ही पढ़ते थे। हिंदीभाषी हिंदी माध्यम से पढ़ते थे तो अन्य भाषा-भाषी अपने राज्य की भाषा में,लेकिन अब बड़े शहरों और कस्बों की बात तो छोड़िए छोटे-छोटे गांवों तक ‘सेंट’ नाम वाले अधकचरे अंग्रेजी विद्यालयों की भरमार हो चुकी है। अंग्रेजी नाम वाले ऐसे-ऐसे सैंटों के नाम पर विद्यालय हैं,जो कभी पैदा ही नहीं हुए। हालांकि,अब कस्बाई विद्यालयों के नामों में कुछ हिंदी नाम वाले सैंट भी जुड़ने लगे हैं,जैसे सैंट राधे-श्याम पब्लिक स्कूल, सैंट भोलाराम पब्लिक स्कूल आदि। जब मैंने पूछा कि यार अपने लोगों को अंग्रेजी सैंट क्यों बनाने लगे,तो वे बताते हैं,साहब स्कूल तो नाम,ड्रेस और चमक-दमक पर ही चलता है। सैंट नहीं लगाएँगे तो अंग्रेजी माध्यम की खुशबू नहीं आएगी। पढ़ाई कौन देखता है ?
अपवाद हो सकते हैं लेकिन सत्य तो यही है कि अपनी भाषा के विद्यालय में वही बच्चे जा रहे हैं,जिनके पास कोई और रास्ता नहीं। अपनी भाषा के तमाम समर्थक भी तो यही करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाषा प्रेम ढोंग है या देश के तमाम लोग अंग्रेजों के जाने के बाद अचानक अंग्रेजी के दीवाने हो गए। वजह बड़ी स्पष्ट है कि,उच्च शिक्षा,रोजगार,व्यापार,व्यवसाय,कानून-न्याय सहित प्रगति के तमाम रास्ते धीरे-धीरे अंग्रेजीमय होते गए। ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रगति की सभी राहों पर अंग्रेजों की तरह आजादी के बाद अंग्रेजी काबिज होती गई। ज्ञान-विज्ञान सहित तमाम क्षेत्रों में हम लगभग पूरी तरह अंग्रेजों पर और उसके चलते अंग्रेजी पर आश्रित होते गए। आजादी के बाद भाषा के क्षेत्र में अगर कुछ बदला आया तो वह भारतीय भाषाओं के प्रतिकूल और अंग्रेजी के पक्ष में ही गया। आम आदमी के पास कोई विकल्प ही न था। फिर जो अंग्रेजी माध्यम से निकल कर आए,अंग्रेजी की वर्चस्ववादी ठसक के साथ जिस भी क्षेत्र में गए,उन्होंने वहाँ भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदी और भारतीय भाषाओं के नाम पर तमाम अकादमियाँ ललित साहित्य,कहानी-कविता से आगे सोचने को ही तैयार न थी। समाज में भी ऐसा वातावरण बना कि कविता-कहानी,गीत-संगीत और मनोरंजन में हिंदी ही हिंदी का विकास व प्रसार है। नतीजतन शिक्षा में,हिंदी अकादमियों और हिंदी सेवी संस्थान अपनी ढपली बजाते रहे और हिंदी हर क्षेत्र से कटती रही। आज भी वही हो रहा है,कुछ भी तो नहीं बदला।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यर्वेदिक विद्यालयों की स्थापना हिंदी माध्यम शिक्षा के लिए की थी। मैं भी ऐसे विद्यालय में अध्यापक रहा,लेकिन अब उनमें से ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम में तब्दील हो गए हैं या बंद हो गए। यह स्थिति हिंदी की ही नहीं बल्कि इसकी तमाम भारतीय बहनों की है। अंग्रेजों की `फूट डालो शासन करो` की नीति का अनुसरण होता रहा,हमारी भाषाएँ आपस में लड़ रही थीं और अंग्रेजी हर क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को लीलते हुए बढ़ रही थी। भाषाओं के सेनानी साहित्यिक विमर्श से अपनी भाषाओं की हवाई तलवारें भांज रहे थे।
संगोष्ठियों और सम्मेलनों के भाषायी अनुष्ठानों में जो विद्वान ऊंची आवाज में विश्व में विभिन्न देशों में हिंदी शिक्षण और हिंदी प्रसार के लंबे-चौड़े आँकड़े पेश करते हैं,यदि उनकी पड़ताल की जाए तो सच्चाई कुछ ही देर में स्पष्ट होने लगती है। स्वभाविक भी है,हिंदी की जड़ें तो भारत में है,जब भारत में ही हिंदी का वृक्ष सूखता जा रहा है तो हम कैसे यह उम्मीद करें कि यहां से बाहर गई टहनियां और अधिक फल-फूल रही होंगी, पर हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं का विकास या प्रसार तभी संभव है,जब अपनी जमीन पर पुष्ट और विकासोन्मुखी हों। निश्चित रूप से हमें विश्व स्तर पर अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि,अपनी विपुल जनसंख्या के कारण भारतवंशी देश और दुनिया के कोने-कोने में फैले हैं और उनमें से अधिकांश को अपनी मातृभूमि और मातृभाषा से प्यार भी है। वे तमाम बाधाओं के बीच अपने धर्म-संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें हिंदी और मातृ-भाषाएं सिखाने के लिए प्रयत्नशील हैं।
दो वर्ष पूर्व विश्व `हिंदी दिवस` पर ‘वैश्विक हिंदी सम्मेलन’ द्वारा एक महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया,जिसमें कई देशों के भारतवंशी हिंदी के विद्वानों ने विदेशों में हिंदी शिक्षण और हिंदी के प्रसार का ब्यौरा रखा और स्पष्ट रुप में यह बताया कि वहां पर भी हिंदी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अनेक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से यहां पधारीं दक्षिण अफ्रीका हिंदी शिक्षा संघ की अध्यक्ष प्रो. उषा शुक्ला ने भी बताया कि उनके देश में भी विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग बंद होते जा रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय में वे हिंदी पढ़ाती थीं वहाँ से हिंदी विषय समाप्त होने पर वे सेवानिवृत्ति तक अंग्रेजी पढ़ाने को विवश थीं। जब हम स्वयं को सम्मान न दें,अपनी भाषाओं को स्वीकार न कर सकें तो दूसरे देशों से ऐसी अपेक्षा बेमानी है। कई देशों में हिंदी मंदिरों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए पढ़ाई जा रही है। कई विश्वविद्यालयों में जहां हिंदी के विभाग हैं,वहां पर हिंदी के विद्यार्थी ढूंढने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर होती है,जो अपनी नौकरी को बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को तलाशते हैं। भारत में भी अनेक स्थानों पर अब ऐसी ही स्थिति आ गई है।
चौंकाने वाली बात यह भी है कि,भारत में हिंदी के नाम पर सरकारी और गैर सरकारी जितनी संस्थाएं,संसाधन,सम्मान आदि हिंदी साहित्य के लिए हैं उसके मुकाबले भाषा के प्रसार के लिए प्रयासरत कार्यों व हिंदी सेवियों के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर अपने भविष्य को दांव पर लगा कर जीवनभर हिंदी के लिए संघर्ष किया या कर रहे हैं। उनमें से शायद ही किसी को किसी स्तर पर कोई प्रोत्साहन,सम्मान या पहचान दी गई हो। हिंदी सेवा के नाम पर भी घूम फिर कर कहानी-कविता वाले ही होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे कई ऐसे वरिष्ठ विद्वान और वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने हिंदी की न केवल लड़ाई लड़ी,बल्कि उच्च स्तरीय ज्ञान-विज्ञान की मौलिक पुस्तकें भी हिंदी में लिखीं,लेकिन उनकी गिनती हिंदीसेवियों में नहीं होती। आए-दिन विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठापन के लिए सरकार,संस्थाओं और अनेक सरकारी और निजी क्षेत्र की कम्पनियों से जूझ रहे लोग भी इनकी परिभाषा में ‘हिंदी सेवी’ नहीं हैं। इसका परिणाम हिंदी के प्रयोग-प्रसार के लिए प्रयासरत लोगों की संख्या बहुत ही कम है,लेकिन इसके बावजूद ये मुट्ठीभर लोग तमाम बाधाओं से जूझते हुए हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठापन की जंग लड़ रहे हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि,किसी भी समाज और उसकी भाषा के विकास के लिए ललित साहित्य अति महत्वपूर्ण है। निश्चय ही साहित्य पाठक की संवेदनाओं को मांझता है। भाषा का विकास करता है,उसे परिमार्जित करता है,लेकिन उसे बचाता नहीं है,और आज जब हर क्षेत्र में अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी अपने अस्तितत्व की लड़ाई लड़ रही है और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी,पाठक और श्रोता बढ़ती आबादी के बावजूद सिमटते जा रहे हैं,तो भाषा का विकास भी कैसे होगा ?
किसी भाषा के प्रसार में उस भाषा के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज देश के तमाम हिंदी के बड़े-बड़े अखबार अपने को आधुनिक और प्रगतिशील दिखाने के लिए हिंदी को अंग्रेजीमय करने को आतुर हैं। हम अपनी आँखों के सामने रोज देख रहे हैं कि किस प्रकार हिंदी के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में बैठे लोग हिंदी के चलते-फिरते जीते-जागते शब्दों के स्थान पर चुन-चुनकर अंग्रेजी के शब्द बैठा रहे हैं। अगर यूँ कहा जाए कि वे हर दिन हर चलते-फिरते जीते-जागते हिंदी शब्द की हत्या करने पर आमादा हैं तो अनुचित न होगा। यही नहीं,अब तो देवनागरी लिपि के स्थान पर हिंदी के अखबार संक्षिप्तियाँ और अनेक शब्दों को रोमन लिपि में भी लिखने लगे हैं,और हम केवल यशोगान कर हिंदी को महिमामंडित कर उसके सामने मौजूद खतरों से नजरें चुरा कर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं।
हिंदी के तमाम साहित्यिक कार्यक्रम और संगोष्ठियों पर भी यदि एक बार भी नजर डालें तो साफ दिखाई दे जाता है कि,उसमे बैठे ज्यादातर लोग ५० वर्ष या उससे अधिक के हैं,और जो कुछ युवा चेहरे हैं भी तो वे हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षकों द्वारा बैठाए गए हैं,लेकिन हम फिर भी बड़े गर्व से सीना ठोंक कर कह रहे हैं कि हिंदी बढ़ रही है,तेजी से बढ़ रही है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी की अधिकांश प्रतिष्ठित पत्रिकाएं पिछले कई दशकों में बंद हो चुकी हैं। संख्या की दृष्टि से आज भी भले ही हिंदी पत्रिकाओं की बड़ी तादाद हो,लेकिन उनकी स्थिति से कौन परिचित नहीं है। अभी भोपाल में पत्रिकाओं के ऐसे ही कार्यक्रम में जो रोचक जानकारियां मिली कि,सैंकड़ों पत्रिकाएं कुछ कविता-कहानी छाप कर इधर-उधर बांट कर सरकारी अनुदान या चंदे आदि के माध्यम से जीवित हैं।
जब जनमानस भाषा से कटेगा तो उसका साहित्य कैसे चलेगा ? पुरस्कार,नाम और पदोन्नति आदि के लिए हिंदी कहानी-कविता,समीक्षा आदि की पुस्तकें भी खूब छप रही हैं, लेकिन उनके पाठक कहाँ बचे हैं ? उनके पाठक या तो विद्यार्थी हैं जो पाठ्यक्रम के कारण पढ़ते हैं,या वे सरकारी पुस्तकालयों में खपती हैं या मुफ्त बंटती हैं। वहाँ भी कितनी पढ़ी जाती हैं,यह भी किसी से छिपा नहीं। यहाँ तक कि पुस्तक विमोचन पर उस पर बोलनेवाले वक्ता भी अक्सर उसे पढ़ कर नहीं आते। हमें सच का सामना करना पड़ेगा,उसे साफगोई से स्वीकारना भी होगा। और उससे निपटने के लिए रणनीति बना कर ठोस प्रयास भी करने होंगे,लेकिन इसके लिए मुट्ठीभर सिपाही बिना हथियार केवल मनोबल से कब तक और कितना लड़ाई लड़ पाएंगे,यह तो वक्त बताएगा लेकिन अंग्रेजी के तेज बहाव के बावजूद जिस प्रकार कुछ लोग पुरजोर ढंग से हिंदी या भारतीय भाषाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं,वह उत्साह पैदा करती है। भारतीय भाषाओं के लिए नि:स्वार्थ भाव से संघर्षरत लोगों को भी प्रोत्साहित कर,उन्हें नायकत्व प्रदान करें ताकि नई पीढ़ी के लोग उनका अनुसरण कर सकें। ‘वैश्विक हिंदी सम्मेलन’ द्वारा इस दिशा में प्रयास किए गए और किए जा रहे हैं,लेकिन वे आटे में नमक के बराबर भी नहीं, इसकी अपनी क्षमता व सीमाएँ हैं। इस दिशा में अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।
२०१४ में मुंबई में ‘वैश्विक हिंदी सम्मेलन’ में भारतीय भाषाओं के प्रसार के संबंध में मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा ने जो कहा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा -‘जो भाषा हृदय की और पेट की भाषा होती है,वही चलती है।‘ मुझे तो लगता है जो पेट की भाषा होती है, वह हृदय को भी भाती है,लेकिन भारत में हिंदी सहित हमारी तमाम भाषाएँ पेट से यानी रोजगार से दूर होने के चलते शिक्षा से और इस प्रकार हमसे दूर हो रही हैं। इसलिए अब वे न तो नई पीढ़ी के हृदय की भाषा हैं और न पेट की। कहा गया है कि पेट के जरिए किसी के हृदय तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए हमें अपनी भाषाओं को बचाना है और आगे बढ़ाना है तो उसका रास्ता भी पेट से यानी रोजगार और प्रगति के मार्ग से हो कर ही निकलेगा।
आवश्यकता इस बात की है कि वे सब लोग जो हिंदी सहित तमाम भारतीय भाषाओं को लेकर चिंतित हैं या कुछ करना चाहते हैं वे कविता -कहानी से आगे बढ़ कर भी देश के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए इनके प्रयोग की दिशा में जनमत तैयार करते हुए प्रयास करें,आवाज़ उठाएं,जगें और जगाएं। साहित्यकार भी इस संघर्ष में अपना योगदान दें। भाषाएँ हैं,तो उनका साहित्य है। दूसरी बात यह कि ललित साहित्य से इतर ज्ञान-विज्ञान,वाणिज्य आदि विभिन्न क्षेत्रों के साहित्य को भी आगे बढ़ाएं व स्वीकारें। मेरा यह मानना है कि सभी भारतीय भाषाएं मिलकर आगे बढ़ेंगी,तो बात बनेगी। हम मिलकर प्रयास करेंगे तो ही हम अपनी भाषाओं को बचा सकेंगे और इन्हें आगे बढ़ा सकेंगे। सभी मित्रों से विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक युवाओं और अन्य भाषा भाषियों को इस अभियान से जोड़ने में भी अपना सहयोग दें। विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापक और प्राध्यापक इसमें काफी सहयोग कर सकते हैं। मेरा अनुरोध केवल भाषा-शिक्षकों से नहीं,सभी विषयों के शिक्षकों से है। मैं बिना किसी का नाम लिए उन सभी व्यक्तियों को नमन करना चाहूंगा,जो हिंदी के प्रयोग और प्रसार को बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर बिना किसी लाभ और लोभ के यथासंभव अधिकाधिक प्रयास कर रहे हैं। यह भी प्रसन्नता की बात है कि देश के अनेक वरिष्ठ विद्वान और भाषाप्रेमी इस अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं।